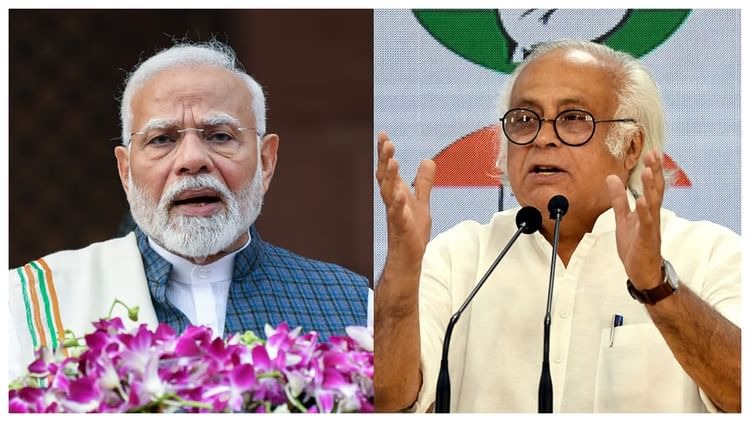नई दिल्ली 7 नवंबर 2025
नई दिल्ली / अहमदाबाद — सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में शुक्रवार को जो स्वर उभरा, उसने केवल एक परिवार के शोक को नहीं छुआ बल्कि पूरे विमानन-तंत्र और सार्वजनिक आशंका पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अहमदाबाद में हुई दर्दनाक एयर इंडिया दुर्घटना के बाद मृतक कमांडर के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने पिता को सांत्वना दी और कहा कि “आप यह बोझ अपने ऊपर न लें — किसी को भी इस हादसे का सिरमौर मानकर दोष देना ठीक नहीं।” अदालत ने यह स्पष्ट किया कि प्रारंभिक AAIB रिपोर्ट में किसी तरह की सीधी निंदा पायलट के लिए दर्ज नहीं की गई है और मीडिया रिपोर्टिंग में जो निर्णायक ताने-बाने बने उन्हें भी न्यायालय ने ‘नैस्टि’ कहकर खारिज किया। अदालत ने केंद्र और नागरिक उड्डयन नियामक को नोटिस जारी कर मामले की जाँच की पारदर्शिता पर सवाल उठाए जाने पर जवाब तलब किया है।
हादसे की तकनीकी पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया जाए तो AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट ने संकेत दिया कि टेक-ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों में ईंधन-वितरण कटने के स्वरूप मिले — और रिकॉर्डिंग में एक पायलट ने दूसरे से ‘क्या आपने फ्यूल कट ऑफ किया?’ जैसा प्रश्न पूछा गया। पर यही बातें स्वतंत्र रूप से पढ़ी जाएँ तो केवल ‘कॉकपिट संवाद’ को पूरे हादसे का निर्णायक कारण मान लेना जल्दबाज़ी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में सिस्टमिक कारणों — रनवे की विशेषताओं, एयरलाइन के रखरखाव और SOP, विमान-निर्माता के डिज़ाइन एवं चेतावनी-सिस्टम की कड़ी जाँच आवश्यक होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही रेखांकित किया कि जांच का उद्देश्य दोषियों की तलाश मात्र नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति रोकने का ठोस उपाय ढूँढना होना चाहिए।
फिलहाल यह भी सच्चाई है कि सार्वजनिक-राजनीतिक व्यवहार में ‘मानवीय त्रुटि’ को घटना का तात्कालिक और सरल कारण मान लेना बहुत सुविधाजनक होता है। जब कोई व्यक्ति मर चुका हो — और वह पायलट-इन-कमांड जैसा प्रतिष्ठित और अब स्वयं जवाब न दे सके — तो संस्थागत और प्रशासनिक भूलों की जाँच छिप सकती है। लंबे समय से आलोचक यही कहते आए हैं कि दुर्घटनाओं के बाद जो प्रक्रिया चलती है उसमें प्राथमिक रूप से ‘किसी एक व्यक्ति’ को कोस देना व्यवस्था के लिए सस्ता और सुरक्षित विकल्प बन जाता है — क्योंकि इससे तकनीकी, वित्तीय और नियामक सवालों की उलझनें पर्दे में चली जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के मौखिक आश्वासन ने थोड़ी राहत दी है, पर इसने वही पुराने सवाल फिर खुलकर रखा है — क्या सरकार और संस्थान हर बड़े हादसे के मामले में ‘सिस्टम की गलती’ की जगह पहले से तय किसी एक martyrs-शरीर को बलि चढ़ाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं?
यह प्रवृत्ति सिर्फ़ संवेदनात्मक नहीं, बल्कि राजनीतिक व नैतिक जोखिम भी बन जाती है। जब जांच-रिपोर्टों, नियामकीय जवाबदेही और मीडिया-रिपोर्टिंग के तर्क-तत्वों पर संदेह पैदा हो जाता है, तो जनता के सामने सरकार की जवाबदेही का प्रश्न खड़ा हो जाता है। आलोचक कहते हैं कि यदि प्रत्येक बड़ी दुर्घटना के बाद “एक मर चुका बलि का बकरा” ही सामने ला दिया जाए — जिसका न तो सक्रिय बचाव करने का अवसर रहता है और न अपनी सफाई देने का — तो वह व्यवस्था की वास्तविक कमियों को उजागर होने से रोक देता है और भविष्य में वह व्यवस्था वही गलतियाँ दोहराती रहती है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इंगित की — जांच केवल अपराध सिद्धि की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह सुधार और रोकथाम का भी मार्ग प्रशस्त करे।
अंततः, पिता को दिए गए न्यायालयीन शब्द — “अपने ऊपर बोझ मत लीजिए” — भावनात्मक रूप से सांत्वना हैं, पर साथ ही यह एक चेतावनी भी है: सार्वजनिक और संस्थागत स्तर पर ‘दोषारोपण-रिफ्लेक्स’ को रोकना होगा। अगर नहीं तो अगली दुर्घटना पर भी किसी न किसी मृतक-व्यक्ति को प्रमुख दु:ख-प्रवर्तक मानकर मामला बंद कर दिया जाएगा — और सिस्टम वही रहेगा। इसीलिए न्यायालय द्वारा केंद्र और DGCA को नोटिस भेजकर स्वतंत्रता और पारदर्शिता की माँग करना सिर्फ़ एक कानूनी कदम नहीं, बल्कि उस बड़े लोकतान्त्रिक सवाल की शुरुआत है — क्या हमारी संस्थाएँ सचमुच सीखने और सुधार करने के लिए गंभीर हैं, या हर बार एक ‘मर चुके बकरे’ को तैयार रखकर मामला टाला जाएगा?