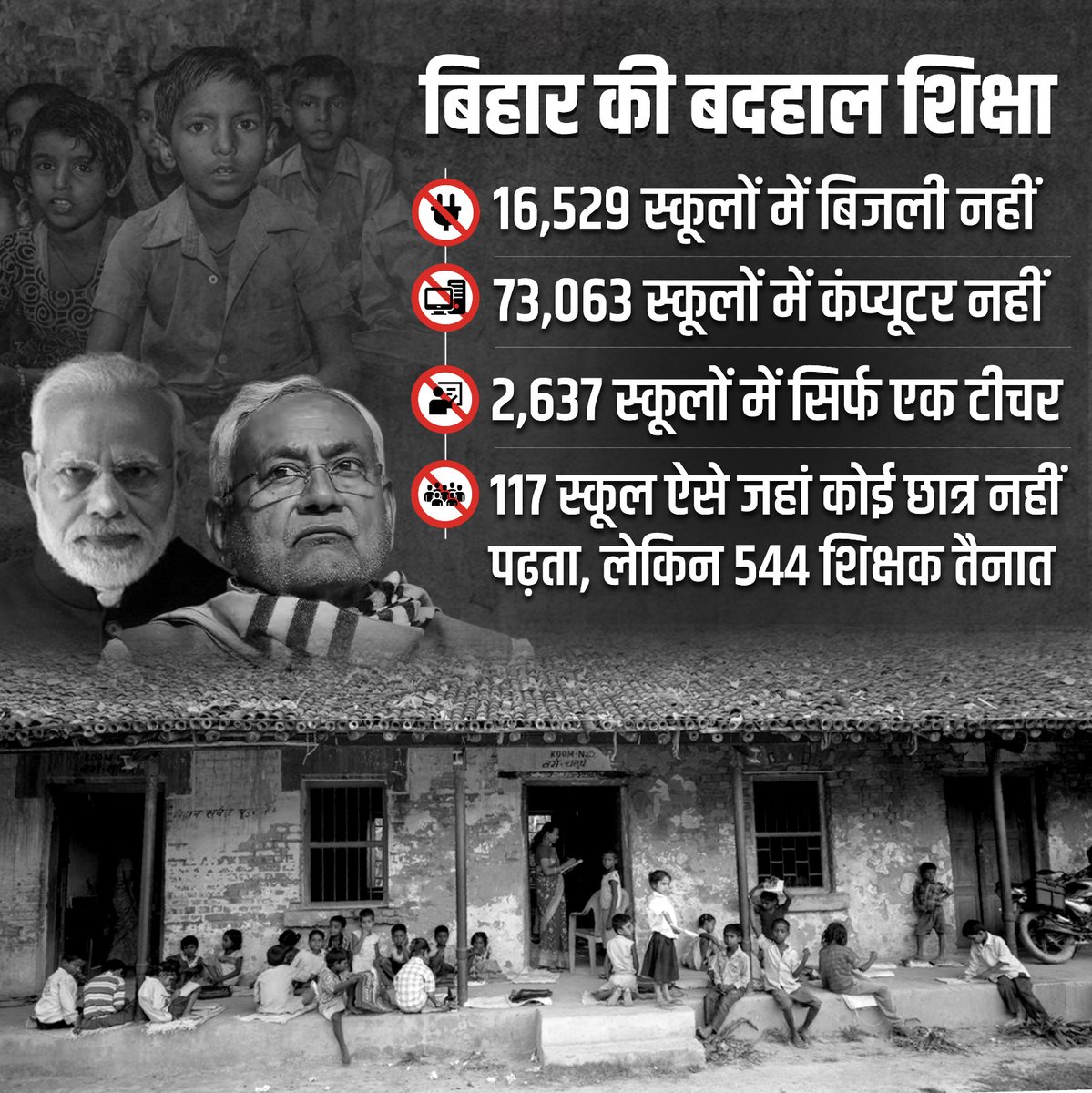प्रोफेसर निपुणिका शाहिद, असिस्टेंट प्रोफेसर, मीडिया स्ट्डीज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी दिल्ली NCR
नई दिल्ली 19 अक्टूबर 2025
वैश्विक दृश्यता की कमी: कहानियों में भागीदारी बनाम वास्तविकता
कहानियाँ समाज की चेतना को आकार देती हैं, पर प्रश्न यह है कि अरबों कहानियों के इस सागर में, उन 1.3 अरब लोगों की ज़िंदगी को कितनी जगह मिलती है जो किसी न किसी प्रकार की विकलांगता / दिव्यांगता के साथ जीते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दुनिया का हर छठा व्यक्ति किसी न किसी रूप में विकलांग है। भारत में भी यह संख्या अनुमानित रूप से 5 से 7 करोड़ के बीच है। यह आँकड़ा स्पष्ट करता है कि यह समूह समाज का एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बावजूद, जब हम मीडिया खपत की बात करते हैं, तो प्रतिनिधित्व का यह अनुपात नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यूनेस्को (UNESCO) की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि विश्व स्तर पर विकलांगता से संबंधित सामग्री 2% से भी कम है।
यह न केवल दृश्यता की कमी को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि मौजूद सामग्री में से ज़्यादातर कहानियाँ दया, चैरिटी या सतही “प्रेरणा” के दृष्टिकोण से दिखाई जाती हैं। यानी, मीडिया उन्हें एक ‘विषय’ या ‘भावनात्मक उपकथा’ तो मानता है, लेकिन ‘शक्ति’ या ‘समान भागीदार’ के रूप में नहीं। इस विशाल वैश्विक अंतर को पाटने के लिए, मीडिया को अपनी कहानी कहने की प्राथमिकता और दृष्टिकोण को बदलने की सख्त ज़रूरत है, ताकि वह सच्ची समावेशिता का आईना बन सके।
प्रतिनिधित्व का संकट: असली आवाज़ों को ग़ायब करना
दशकों तक, मीडिया ने विकलांगता को एक “संघर्ष” या “चमत्कार” की कहानी के रूप में दिखाया, जो अक्सर एक जटिल मानवीय अनुभव को एक सरल और भावनात्मक प्रतीक में बदल देता है। समस्या केवल मात्रा की नहीं, बल्कि गुणवत्ता और प्रामाणिकता की भी है। Annenberg Inclusion Initiative (2022) के एक अध्ययन के अनुसार, लोकप्रिय फ़िल्मों में केवल 2.4% बोलने वाले पात्र विकलांगता का प्रतिनिधित्व करते हैं—यह एक गंभीर अंडर-रिप्रेजेंटेशन है। इससे भी अधिक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इन किरदारों में से 95% को ग़ैर-विकलांग अभिनेता निभाते हैं। यह आँकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि असली आवाज़ें और कलाकार अब भी पर्दे से दूर रखे जा रहे हैं, और उनके स्थान पर ‘आउटसाइडर्स’ बोल रहे हैं। CODA (2021) जैसी फ़िल्में, जिसने ऑस्कर जीता, इस पैटर्न को तोड़ती हैं, क्योंकि इसने विकलांगता को “प्रेरणादायक” के बजाय “सामान्य” और वास्तविक दिखाया।
भारत में ब्लैक, तारे ज़मीन पर, सितारे जमीन पर या श्रीकांत जैसी फ़िल्में उस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रतीक हैं जहाँ सिनेमा अब समावेश की भाषा सीख रहा है। ये कृतियाँ स्थापित करती हैं कि प्रतिनिधित्व केवल दिखना नहीं है—यह कलाकारों और समुदायों के लिए गरिमा, रोज़गार और समानता का अधिकार है। जब हम प्रामाणिक कलाकारों को चुनते हैं, तो हम केवल एक भूमिका नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सामाजिक संदेश को सामने लाते हैं।
मीडिया की नैतिक ज़िम्मेदारी और पहुँच का अधिकार
मीडिया की शक्ति केवल दुनिया को दिखाने की नहीं है, बल्कि उसे बदलने की है। समावेशी कहानियों का युवाओं पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है: Harvard Kennedy School के एक शोध में पाया गया कि समावेशी कहानियों से युवाओं में सहानुभूति और संवेदनशीलता 40% तक बढ़ जाती है। यह दर्शाता है कि मीडिया संवेदनशीलता बढ़ाने का एक अचूक उपकरण है। हालाँकि, मुख्यधारा का मीडिया अक्सर अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी से पीछे हट जाता है, जहाँ रिपोर्टिंग अब भी नीति, शिक्षा या रोज़गार के बजाय “दया-भाव” और “प्रेरक उपलब्धियों” पर केंद्रित रहती है। यह भाषा सामाजिक दूरी को मिटाने के बजाय और गहरा करती है।
इससे भी बड़ा मुद्दा पहुँच (Accessibility) का है, जिसे सुविधा नहीं, बल्कि अधिकार माना जाना चाहिए। Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), जिस पर भारत ने 2007 में हस्ताक्षर किए, स्पष्ट कहता है कि सूचना और संचार तक समान पहुँच हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इसके बावजूद, Centre for Internet and Society (2023) की रिपोर्ट बताती है कि भारत में केवल 10% OTT प्लेटफ़ॉर्म्स ही अपनी सामग्री में सबटाइटल, ऑडियो डिस्क्रिप्शन या सांकेतिक भाषा जैसी सुविधाएँ देते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमारी 90% डिजिटल कहानियाँ आज भी लाखों लोगों को पीछे छोड़ रही हैं। विश्व बैंक के अनुसार, जिन देशों ने समावेशी मीडिया और शिक्षा में निवेश किया है, वहाँ विकलांग व्यक्तियों की रोज़गार भागीदारी 7% तक बढ़ी है। इससे साबित होता है कि समावेश केवल नैतिक नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति का भी एक शक्तिशाली मार्ग है।
दृश्यता से आवाज़ तक: डिजिटल भविष्य और समावेशी पत्रकारिता
मीडिया कवरेज की मात्रा और विषयवस्तु दोनों में गंभीर असंतुलन है। UNESCO की 2023 ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग रिपोर्ट बताती है कि विकलांगता से जुड़ी खबरें कुल मीडिया कवरेज का 2% से भी कम हैं, और उनमें से लगभग 70% केवल इवेंट-आधारित होती हैं—जैसे पुरस्कार या चैरिटी। भारत में, Centre for Disability Studies, हैदराबाद (2019) के अध्ययन में पाया गया कि प्रमुख अखबारों के 5,000 फ्रंट-पेज लेखों में से केवल 12 लेख ही विकलांगता अधिकारों या नीतियों पर केंद्रित थे।
यह स्पष्ट करता है कि पत्रकारिता का ध्यान “क्या हो रहा है” (इवेंट) पर है, न कि “क्या होना चाहिए” (अधिकार, नीति) पर। भविष्य की दिशा डिजिटल समावेशन में निहित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), कैप्शनिंग टूल्स और वॉइस-बेस्ड तकनीकें मीडिया को सभी तक पहुँचाने में क्रांति ला सकती हैं। हम एक ऐसे न्यूज़रूम की कल्पना कर सकते हैं जहाँ AI तुरंत सबटाइटल तैयार करे, जिससे 90% डिजिटल खाई को पाटा जा सके। यूनेस्को की 2024 की रिपोर्ट ने भी जोर दिया है कि वैश्विक मीडिया कवरेज का 2% से भी कम हिस्सा ही विकलांगता से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है, और प्रगति अब भी असमान है। We Care Film Festival l, Purple film festival जैसी पहलें, जो 40 देशों की 200 से अधिक फ़िल्मों को मंच दे चुकी हैं, इस कथा को बदल रही हैं। मीडिया के सामने चुनौती अब केवल विकलांगता “दिखाने” की नहीं है, बल्कि उसे सटीकता, संवेदना और समान अधिकार के साथ “देखने” की है। अंत में, सच्चा समावेशन नीतियों में नहीं, बल्कि कहानियों में बुना जाता है। जब हम कहानी कहने का तरीका बदलते हैं, तो हम सिर्फ़ कथा नहीं, बल्कि दुनिया बदलते हैं।
विकलांगता: दया का विषय नहीं, आर्थिक और रचनात्मक प्रगति का उत्प्रेरक
मीडिया में समावेश की बहस केवल नैतिक या भावनात्मक सीमाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका सीधा संबंध आर्थिक और रचनात्मक प्रगति से है। अक्सर विकलांगता को एक सामाजिक बोझ या दान का विषय मान लिया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि यह एक विशाल और अप्रयुक्त मानवीय पूंजी है। विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि जिन देशों ने समावेशी मीडिया, शिक्षा और कार्यस्थलों में निवेश किया है, वहाँ विकलांग व्यक्तियों की रोज़गार भागीदारी में 7% तक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि समावेशन केवल समाज को मानवीय नहीं बनाता, बल्कि सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को मज़बूत करता है।
इसके अलावा, प्रामाणिक और विविधतापूर्ण कहानियों को शामिल करना रचनात्मकता को भी बढ़ावा देता है। जब CODA जैसी फ़िल्में (जो कि वास्तविक DEAF समुदाय की आवाज़ को मंच देती हैं) ऑस्कर जीतती हैं, तो वे केवल पुरस्कार नहीं लातीं, बल्कि यह साबित करती हैं कि प्रामाणिक प्रतिनिधित्व व्यावसायिक रूप से सफल और कलात्मक रूप से समृद्ध हो सकता है। इसलिए, मीडिया को विकलांगता को “संघर्ष की कहानी” के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे समूह के रूप में देखना चाहिए जिसकी भागीदारी और अद्वितीय परिप्रेक्ष्य नवाचार और आर्थिक विकास के लिए अपरिहार्य हैं।
डिजिटल असमानता: पहुँच का अधिकार और AI का भविष्य
आज के दौर में सूचना और संचार तक पहुँच (Accessibility) किसी सुविधा या विकल्प का विषय नहीं, बल्कि एक मूलभूत मानवीय अधिकार है। हालाँकि, डिजिटल युग में यह अधिकार भी एक बड़ी असमानता का सामना कर रहा है। Centre for Internet and Society (2023) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में केवल 10% OTT प्लेटफ़ॉर्म्स ही अपनी सामग्री में सबटाइटल, ऑडियो डिस्क्रिप्शन या सांकेतिक भाषा जैसी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि हमारी 90% डिजिटल कहानियाँ जानबूझकर या अनजाने में लाखों लोगों को दरकिनार कर रही हैं।
यह न केवल सामाजिक बहिष्कार है, बल्कि Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) का उल्लंघन भी है। इस खाई को पाटने के लिए, अब हमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी तकनीकों की ओर रुख करना होगा। AI-संचालित कैप्शनिंग टूल्स, वॉइस-बेस्ड तकनीकें, और स्वचालित सांकेतिक भाषा अनुवाद मीडिया की पहुँच में क्रांति ला सकते हैं। मीडिया उद्योग को इसे तकनीकी चुनौती के बजाय नैतिक अनिवार्यता के रूप में प्राथमिकता देनी चाहिए। डिजिटल समावेशन ही वह अगला कदम है जो यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में हर कहानी को, हर डिवाइस पर, हर व्यक्ति द्वारा सुना और समझा जा सके।