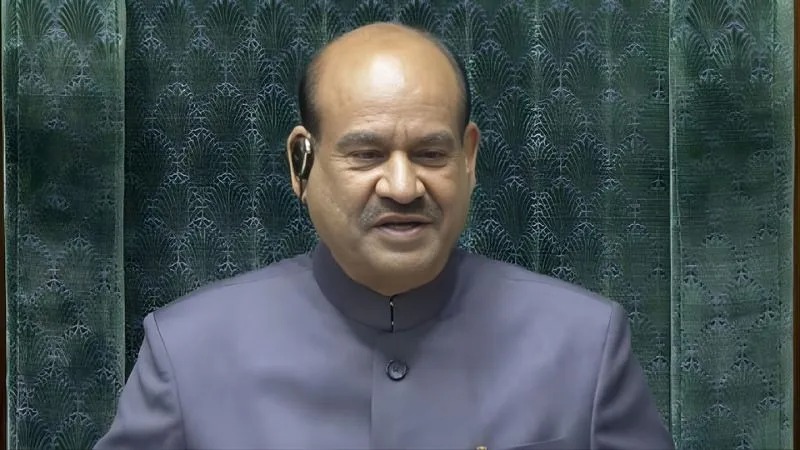डॉ शालिनी अली, समाजसेवी | नई दिल्ली 12 अक्टूबर 2025
जड़ों की पुकार — हमारी पहचान की असली मिट्टी
यह एक शाश्वत सत्य है कि मनुष्य चाहे कितनी भी भौतिक प्रगति कर ले, कितनी भी ऊँची उड़ान भर ले, उसकी असली और मौलिक पहचान हमेशा उसकी जड़ों से ही जुड़ी रहती है। ये जड़ें केवल पैतृक स्थान या वंशावली का प्रतीक नहीं होतीं; ये वे अदृश्य आधारशिलाएँ हैं जो व्यक्ति के भीतर संस्कार, नैतिक संवेदनशीलता और जीवन के आवश्यक संतुलन के बीज बोती हैं। हमारी जड़ें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हैं, हमारा सामूहिक अनुभव हैं, पीढ़ी-दर-पीढ़ी चला आ रहा पारंपरिक ज्ञान हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वह पावन मिट्टी हैं जिसमें बचपन की सहज खुशबू, माँ की अनमोल सीख और समाज का निश्छल अपनापन गहराई से बसा होता है। विडंबना
यह है कि आज का तथाकथित ‘आधुनिक मानव’, तकनीक की तेज़ दौड़ में, ग्लोबल ट्रेंड्स के मोह और डिजिटल आकर्षण के कृत्रिम जाल में फंसकर, अपने ही मूल आधार से धीरे-धीरे कटता जा रहा है। आधुनिकता ने उसे गगन-चुम्बी ऊँचाईयों पर उड़ना तो सिखाया है, मगर ज़मीन से उसका आवश्यक रिश्ता कमज़ोर कर दिया है। यही आज के विकास की सबसे बड़ी विडंबना है — कि भौतिक उन्नति की ऊँचाइयों पर चढ़ते हुए इंसान भावनात्मक और आत्मिक रूप से भीतर से बौना और खाली होता जा रहा है।
आधुनिकता का जाल — चमक के पीछे की गहन थकान
वर्तमान जीवनशैली का विरोधाभास स्पष्ट है: हमारा जीवन आज सुविधाओं और भौतिक संसाधनों से पूरी तरह भरा हुआ है, परंतु उसमें आत्मिक शांति और संतोष का नितांत अभाव है। एक छोटा सा स्मार्टफोन हमें पूरी दुनिया को अपनी हथेली में समेट लेने का भ्रम तो देता है, लेकिन यही डिजिटल उपकरण हमारी आत्मा और चेतना को अनगिनत दिशाओं में बिखेर देता है। सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को यह झूठा आभास दिया है कि वह दुनिया से “जुड़ा हुआ” है, जबकि वास्तविकता यह है कि लोग वास्तविक जीवन में पहले से कहीं अधिक अकेले, पृथक और भावनात्मक रूप से खंडित हैं। हर सुबह “अपडेट” और “अपग्रेड” की अनवरत, अंतहीन भागदौड़ ने इंसान के भीतर की सहज स्थिरता, धैर्य और चिंतनशीलता को छीन लिया है।
परिणामस्वरूप, वह कामयाब तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन वह सफलता उसे अंदर से थका हुआ और बोझिल महसूस कराती है; वह आर्थिक रूप से अमीर तो हो गया है, मगर असंतुष्टि और शून्यता का भाव उसके भीतर गहरा गया है। हर नई सुबह उसका सामना नई और तेज़ मशीनों से होता है, मगर पुराने, गहरे रिश्तों की मानवीय गर्माहट और स्नेह कहीं गुम हो चुका है। आधुनिकता ने निस्संदेह इंसान को तेज़ और कुशल बनाया है, पर इसी प्रक्रिया में उसे संवेदनहीन भी कर दिया है। और यह बढ़ती हुई संवेदनहीनता ही आज के समाज की सबसे बड़ी और मौलिक त्रासदी है।
जापान के Asahi कंपनी की कहानी — जब आधुनिकता को झुकना पड़ा कलम-कागज के सामने
जापान की एक विशाल और मशहूर बियर कंपनी ‘असाही’ (Asahi) पर हाल ही में हुए साइबर हमले की घटना सिर्फ़ एक तकनीकी आपदा नहीं थी, बल्कि यह आधुनिकता की अंधी दौड़ में मानव की संपूर्ण निर्भरता का एक शक्तिशाली प्रतीक थी। साइबर हमले के कारण उनके सारे डिजिटल सिस्टम, जो उनकी पूरी कार्यप्रणाली का आधार थे, एक पल में ठप हो गए। मशीनरी और नेटवर्क पर पूरी तरह निर्भर यह दिग्गज कंपनी अचानक एक ऐसे चौराहे पर आ खड़ी हुई, जहाँ उसे मजबूरन वही करना पड़ा जो दशकों पहले किया जाता था — उन्हें अपनी कार्यप्रणाली को सरल बनाते हुए, कागज़ और कलम के बुनियादी औजारों पर वापस लौटना पड़ा। यह घटना उस भविष्य का एक गंभीर पूर्वाभास है, जहाँ इंसान की अपनी ही बनाई हुई जटिल मशीनें, किसी विफलता के क्षण में, उसे उसके मानवीय मूल, उसकी सरलता और स्थिरता में लौटने पर बाध्य कर देती हैं।
यह हमें याद दिलाती है कि आधुनिकता कितनी भी दुर्दम्य और शक्तिशाली क्यों न हो जाए, मानवता का मूल आधार हमेशा सरलता, स्थिरता, सहज बुद्धि और प्राकृतिक विवेक ही रहेगा। कभी-कभी किसी बड़े “सिस्टम फेलियर” के बहाने ही प्रकृति हमें यह आवश्यक सबक सिखाती है कि हमारा असली और सबसे मजबूत “बैकअप” हमारे भीतर ही मौजूद है — और वह है हमारा मानवीय स्पर्श, हमारा विवेक, हमारा कागज़, और हमारी कलम की शक्ति।
टूटते रिश्ते और बिखरता मन — तकनीकी युग का मौन संकट
इंसान ने वैज्ञानिक पराकाष्ठा हासिल करते हुए चाँद पर अपना राष्ट्रीय झंडा गाड़ दिया है, पर अपने ही पड़ोसी का हाल पूछने की मानवीयता भूल गया है। हमने कृत्रिम बुद्धि वाले जटिल ‘चैटबॉट्स’ का निर्माण कर लिया है, पर वास्तविक मानवीय बातचीत की स्वाभाविक गर्माहट और गहराई को खो दिया है। हमारे पास आज ‘डेटा’ का अथाह भंडार है, पर दिशा का कोई बोध नहीं; हमारे पास ‘जानकारी’ का अम्बार है, पर सच्चे ‘ज्ञान’ का अभाव है। हम 5G और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की गति और रफ्तार में इतने आगे निकल आए हैं कि अब “धीरे चलना”, “रुकना” या “ठहरना” हमें एक अपराध या अक्षमता जैसा महसूस होता है। लेकिन यह प्रकृति का नियम है कि हर तेज़ और उन्मादी दौड़ के बाद एक गहरी शारीरिक और मानसिक थकान आती है।
हर चरम ऊँचाई को छूने के बाद साँस की कमी महसूस होती है। और हर निरंतर शोर के बाद एक गहरी, असहज चुप्पी आती है — वही चुप्पी जिसमें इंसान खुद से, अपनी आत्मा से, मिलने की कोशिश करता है। आज के तकनीकी युग का सबसे बड़ा मौन संकट यह नहीं है कि लोग शारीरिक रूप से मर रहे हैं, बल्कि यह कि वे जीवन के वास्तविक, भावनात्मक सार को जीना भूल रहे हैं। वे तकनीकी रूप से तो जीवित हैं, पर जीवन के वास्तविक आनंद और अनुभवों से पूरी तरह कटे हुए हैं।
क्या लौटना पीछे जाना है — या खुद को फिर से पाना है?
समाज में “जड़ों की ओर लौटना” को अक्सर रूढ़िवाद, पुरातनता या पीछे जाने के प्रतीक के रूप में लिया जाता है, जबकि वास्तविकता और गहन अर्थ में यह स्वयं को पहचानने, आत्म–पुनर्निर्माण और आत्म-खोज की एक आवश्यक प्रक्रिया है। यह कोई पलायन या हार नहीं है, बल्कि यह चेतना और विवेक का पुनर्जागरण है। जब हम अपनी प्राचीन परंपराओं, अपने शाश्वत नैतिक मूल्यों और जीवन के सरल, सहज सिद्धांतों की ओर लौटते हैं, तो हम सामाजिक दौड़ में पिछड़ते नहीं — बल्कि हम भीतर से स्थिर, मज़बूत और अधिक केंद्रित होते हैं।
यह प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे किसी विशालकाय पेड़ को नई और हरी पत्तियाँ उगाने से पहले, अपनी गहरी जड़ों को पूरी दृढ़ता से सींचना और मज़बूत करना पड़ता है। आज के इस अति-आधुनिक समय में “लौटना” का अर्थ है — अपनी खोई हुई संवेदनशीलता को फिर से जीवित करना, अपनी स्वाभाविक सरलता और निश्छलता को स्वीकार करना, और अपनी मानवता तथा मानवीय मूल्यों को अपनी ज़िंदगी के केंद्र में फिर से स्थापित करना। यह आधुनिकता का अनावश्यक विरोध नहीं है, बल्कि यह उसकी तेज़, बेलगाम रफ्तार पर एक आवश्यक मानवीय संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है।
वापसी की राह — धीमे चलना भी एक क्रांति है
अगर हमें सचमुच इस मौन संकट से बाहर निकलना है, तो हमें अपने जीवन की गति को नियंत्रित करना होगा और जानबूझकर “धीमेपन” को फिर से जगह देनी होगी। कभी-कभी मशीनें और स्क्रीन बंद कर के, अपने हाथों से कागज़ पर लिखना, प्रकृति के शांत वातावरण के बीच ध्यान और समय बिताना, और अपने प्रियजनों से किसी डिजिटल उपकरण के बिना आमने-सामने, पूरे ध्यान से बात करना — यह सब आज के तकनीकी वर्चस्व के ख़िलाफ़ एक नए, मानवीय विद्रोह के रूप हैं।
हमें यह मूलभूत सत्य हमेशा याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में एक शक्तिशाली उपकरण है, न कि हम उसके हाथ में बंधे हुए गुलाम। आधुनिकता की इस निरंतर, बेलगाम दौड़ में अगर हम अपनी आत्मा, अपनी संवेदनशीलता और अपने मानवीय विवेक को खो दें, तो ऐसी भौतिक जीत का आखिर अर्थ ही क्या रह जाता है? जड़ों की ओर लौटना यानी उसी खोई हुई आत्मा, उस विवेक को फिर से हासिल करना है। यह लौटना अतीत की ओर नहीं है — बल्कि यह मानवता की ओर है, जहाँ जीवन की गुणवत्ता गति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
जड़ें हमें रोकती नहीं, थामती हैं
हमें यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि हमारी जड़ें हमारी प्रगति की बेड़ियाँ या अड़चनें नहीं हैं, बल्कि वे हमारी पहचान की मिट्टी की मज़बूत पकड़ हैं — वही पकड़ जो हमें जीवन के बड़े-से-बड़े तूफानों और डिजिटल भटकावों के बीच भी दृढ़ता से टिकाए रखती है। चाहे वह Asahi जैसी विशाल कॉर्पोरेट कंपनियाँ हों या रोज़मर्रा की भागदौड़ में शामिल आम आदमी — हर कोई जीवन में कभी न कभी ऐसी स्थिति में अवश्य आता है, जब उसे यह गहन अहसास होता है कि उसकी असली सुरक्षा और शांति किसी अदृश्य “क्लाउड सर्वर” में नहीं, बल्कि उसके भीतर के गहरे मानवीय और नैतिक “कनेक्शन” में निहित है। शायद अब वह निर्णायक वक्त आ गया है कि हम सभी फिर से याद करें और स्वीकार करें — आधुनिकता हमें भौतिक रूप से आगे बढ़ा सकती है, लेकिन हमारी जड़ें ही हमें आत्मिक रूप से ज़िंदा और इंसान बनाए रखती हैं।
मनुष्य तभी तक इंसान रहेगा, जब उसकी आत्मा किसी डिजिटल कोड या तकनीक से नहीं, बल्कि सच्ची, निश्छल मानवीय संवेदना से संचालित होगी। और शायद यही वह अंतिम और निर्णायक क्षण है जब दुनिया को, समाज को और प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर झाँककर यह प्रश्न पूछना होगा — क्या अब हमें अपनी जड़ों की तरफ और अपनी मौलिक मानवता की ओर लौटना नहीं चाहिए?