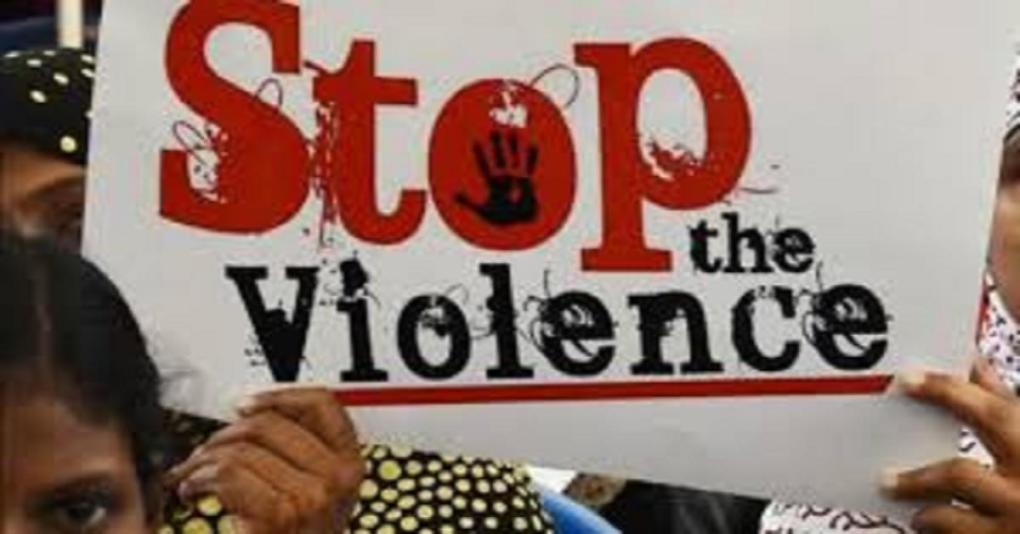विकास के नारों के पीछे दबे उत्पीड़न की चीख़
जब केंद्र की सत्ताधारी सरकार “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” जैसे समरसता के ऊँचे नारों को बुलंद करती हो, और उसी शासनकाल में देश के सबसे वंचित वर्ग, दलितों पर हिंसा, भेदभाव और संरचनात्मक उत्पीड़न का ग्राफ़ लगातार ऊपर चढ़ता दिखाई दे — तो यह स्थिति केवल प्रशासन की सतही कमजोरियों का संकेत नहीं हो सकती, बल्कि इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक और विचारधारात्मक कट्टरता छिपी होने का गंभीर संदेह पैदा होता है। नरेंद्र मोदी की सरकार (2014 से अब तक) के दौरान दलितों पर हुई हिंसा की रिकॉर्ड-तोड़ घटनाएँ, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के सरकारी आँकड़ों, संसद में दिए गए मंत्रालयी उत्तरों, प्रमुख मानवाधिकार समूहों की कठोर रिपोर्टों और मुकदमेबाज़ी की भयानक खामियों का एक विस्तृत जाल एक भयावह तस्वीर खींचता है। यह तस्वीर एक खुली चेतावनी है कि भारत में मनुवादी शक्ति–संरचनाएँ कितनी मजबूत हैं, कितनी मुखर हैं, और किस प्रकार राजनैतिक संरक्षण में वे एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं, जिसने संवैधानिक समानता और न्याय के वादों को खोखला कर दिया है। यह तीन खंडों में किया गया यह गहन विश्लेषण इस क्रूर वास्तविकता को सामने लाता है कि किस प्रकार संस्थागत पक्षपात और राजनीतिक चुप्पी ने दलित समुदाय को निरंतर जोखिम और असुरक्षा के घेरे में धकेल दिया है।
NCRB और संसद के आँकड़े: अपराधों में विस्फोटक उछाल की भयावह तस्वीर
NCRB के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संसद के पटल पर प्रस्तुत किए गए आधिकारिक उत्तरों के अनुसार, देश में दलितों (Scheduled Castes, SCs) के खिलाफ दर्ज होने वाले अपराधों की संख्या में निरंतर और विस्फोटक वृद्धि हुई है। विशेष रूप से, वर्ष 2022 में दलितों के खिलाफ दर्ज अपराधों की संख्या बढ़कर 57,582 हो गई थी, जो कि इससे ठीक पहले के वर्ष 2021 की संख्या 50,900 से लगभग 13.1% अधिक थी।
यह न केवल संख्यात्मक वृद्धि है, बल्कि इसका सीधा असर अपराध दर पर भी पड़ा, जो 2022 में (प्रति लाख आबादी पर) बढ़कर 28.6 हो गई, जबकि 2021 में यह 25.3 थी। इन दर्ज मामलों का वर्गीकरण भी उत्पीड़न के पैटर्न को दर्शाता है, जहाँ अधिकांश अपराध “simple hurt” (सरल चोट) के अंतर्गत दर्ज हुए, जिनकी संख्या 2022 में 18,428 थी। इसके बाद “criminal intimidation” और फिर अंततः PoA Act (SC/ST Prevention of Atrocities Act) के अंतर्गत मामले दर्ज हुए।
राज्य-वार वितरण देखें तो उत्तर प्रदेश (12,287 मामले, कुल का 23.78%), राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे भाजपा-शासित या भाजपा-प्रभावित राज्य इस भयावह सूची में शीर्ष पर रहे। यह एक विचलित कर देने वाला तथ्य है कि लगभग 98% अपराध SC के खिलाफ केवल 13 राज्यों में दर्ज हुए हैं, जो या तो कमजोर रिपोर्टिंग तंत्र या शिकायत दर्ज करने के प्रति पुलिस में विश्वास की कमी को दर्शाता है। ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच (AIDMAM) की रिपोर्ट यह भी कहती है कि 2014–2022 की अवधि में कुल अपराधों में से लगभग 15.32% मामले दलित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ थे, जो दोहरे उत्पीड़न की ओर इशारा करता है।
संस्थागत चुप्पी और न्याय की दुर्बलता: रिपोर्टों की कठोर आलोचना
सरकारी आँकड़ों की यह तस्वीर केवल सतही है, क्योंकि मानवाधिकार संगठनों ने बार-बार यह रेखांकित किया है कि केवल मामले दर्ज करना ही न्याय की गारंटी नहीं है; बल्कि एफआईआर न करना, गवाहों को धमकाना, मुकदमे लटकाना और जानबूझकर जांच में देरी करना जैसी प्रक्रियागत खामियाँ दलितों को न्याय दिलाने में सबसे बड़ी बाधाएँ हैं। यह केवल प्रशासनिक निष्क्रियता नहीं है — कई मामलों में, संस्थागत पक्षपात और जानबूझकर की गई उपेक्षा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) की “Hidden Apartheid” जैसी पुरानी लेकिन प्रासंगिक रिपोर्टों में भी इसी तरह की प्रक्रियात्मक खामियों का वर्णन किया गया है, जो आज भी ज़मीनी हकीकत बनी हुई हैं। कुछ प्रमुख सामाजिक और दलित अधिकार संगठन सीधे तौर पर यह आरोप लगाते हैं कि भाजपा-शासन वाले राज्यों में दलित अत्याचार के मामलों की संख्या न केवल अधिक होती है, बल्कि वहां सत्ता और संगठनात्मक समर्थन के कारण मनुवादी ताकतें अधिक मुखर होकर काम कर पाती हैं, क्योंकि उन्हें राजनीतिक दंड का कोई डर नहीं होता।
एनजीओ रिपोर्टों ने यह भी बताया है कि जाति-आधारित हिंसा विशेष रूप से दलित महिलाओं के खिलाफ लैंगिक और सामाजिक उत्पीड़न के रूप में होती है, जिसमें केवल यौन हमले ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक बेइज्जती, सामाजिक कलंक और बड़े पैमाने पर सामाजिक बहिष्कार भी शामिल है। यह संस्थागत पक्षपात, न्यायिक प्रक्रिया को धीमा करके, अपराधी को प्रभावी रूप से बचाने और पीड़ित को हतोत्साहित करने का काम करता है।
मनुवादी सोच का ज़मीनी पैटर्न: ऊना से हाथरस तक की क्रूरता
मोदी सरकार के शासनकाल में हुई कुछ प्रमुख और प्रतीकात्मक घटनाएँ यह दर्शाती हैं कि मनुवादी सोच ने ज़मीनी स्तर पर कितनी क्रूरता और निर्भीकता से काम किया है। 2016 का ऊना कोड़े कांड (गुजरात) इसका प्रतीक बन गया, जहाँ मृत गाय की चमड़ी हटाने के बहाने दलित युवकों को सार्वजनिक रूप से न केवल पीटा गया, बल्कि घटना का वीडियो भी वायरल कर दिया गया, जिसने देशव्यापी आक्रोश और विरोध को जन्म दिया। वहीं, 2020 का हाथरस कांड (उत्तर प्रदेश) ने देश को हिलाकर रख दिया था, जब एक दलित महिला के खिलाफ कथित गैंगरेप हुआ और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।
इस मामले में आरोप लगे कि प्रशासन और पुलिस ने न केवल समय रहते न्याय नहीं दिया, बल्कि परिवार की इच्छा के विरुद्ध रात के अंधेरे में जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया। इन प्रमुख घटनाओं के बीच, स्थानीय स्तर पर रोज़मर्रा की हिंसा (जैसे लाठियों से हमला, भूमि विवाद में संघर्ष, सामाजिक बहिष्कार, पानी या मंदिर/स्कूल में प्रवेश न देना) लगातार दर्ज होती रही, लेकिन उनमें से कई मामले राजनीतिक विमर्श में जगह नहीं बना पाए।
इन घटनाओं का पैटर्न बताता है कि जहां मनुवादी जातियाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभुत्व में हैं, वहां दलितों को चुनौती देना जानलेवा बन जाता है, क्योंकि स्थानीय सत्ता, ज़मींदारी संबंध, और पंचायत तथा पुलिस प्रशासन में प्रभुत्व — ये सभी ताकतें मनुवादी विचारधारा को बनाए रखने और दलितों के विरोध को दबाने में सहायक होती हैं।
भेदभाव और चुप्पी का राजनीतिक तंत्र: सुरक्षा का अभाव
दलितों के खिलाफ अत्याचारों को बढ़ावा देने में भेदभाव और राजनीतिक चुप्पी का एक संगठित तंत्र काम करता है। यह तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि बहुत बार मामलों को PoA Act (Prevention of Atrocities Act) की गंभीर धाराओं के बजाय भारतीय दंड संहिता (IPC) की सामान्य धाराओं में दर्ज किया जाता है, जिससे अपराधी आसानी से बच निकलते हैं।
कई पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज करने से ही मना कर देते हैं या जानबूझकर धाराएँ घटा देते हैं। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि पीड़ित और उनके गवाहों को धमकाया जाता है, और परिवारों पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जाता है, जिसके कारण कई अत्याचार “अन-दर्ज” रह जाते हैं। जब केंद्र या राज्य सरकारें ऐसी गंभीर और प्रतीकात्मक घटनाओं पर कठोर, तत्काल प्रतिक्रिया देने या सार्वजनिक रूप से जवाबदेही सुनिश्चित करने में विफल रहती हैं, तो वह एक स्पष्ट संकेत देती हैं — कि दलितों का विरोध और उपयोगिता राजनीतिक एजेंडे में सीमित है।
जब सत्ता चुप्पी साध लेती है या देरी करती है, तो मनुवादी ताकतें और अधिक मुखर होती हैं और उन्हें अपने कृत्यों के लिए राजनीतिक समर्थन का आभास होता है। इस पूरे परिदृश्य में, दलित महिलाएं जाति और लिंग दोनों पर दोहरी मार सहती हैं, जहाँ यौन अपराधों के मामले अक्सर कम रिपोर्ट होते हैं क्योंकि शर्म, सामाजिक कलंक और न्याय की भयभीत प्रक्रिया उन्हें मौन रहने पर मजबूर कर देती है।
क्या दलितों की सुरक्षा “वैकल्पिक” विषय है?
यह लेख एक आक्रामक चेतावनी और दस्तावेजी-आधार पर खींची गई तस्वीर है, जो यह स्पष्ट करती है कि भारत का संविधान समानता, गैर-भेदभाव और सामाजिक न्याय का वादा करता है, लेकिन व्यवहार में वह असल में सिर्फ एक खोखला बयान बनकर रह गया है। मोदी सरकार द्वारा नारा-स्तर पर “सभी के साथ” का वक्तव्य कुछ प्रतीकात्मक बयानों तक सीमित रह गया है, जबकि ज़मीनी कार्रवाई में दलितों की सुरक्षा पर विराम नहीं लगा है।
NCRB की संख्या, गांव-स्तर की घटनाएँ, और मानवाधिकार रिपोर्टें — ये सभी मिलकर स्पष्ट संकेत देते हैं कि मनुवादी सोच आज भी न केवल जीवित है, बल्कि सशक्त रूप में काम कर रही है। यदि सरकार (न केंद्र, न राज्य) ने अब भी कठोर और त्वरित कदम नहीं उठाए, तो यह स्पष्ट कहलाएगा कि उसका विकास व नीति दलितों पर केवल सुखोद-उन्मुख (lip service) है, न कि न्यायोन्मुख। क्या यही वह लोकतंत्र है जहाँ दलितों की सुरक्षा “वैकल्पिक” विषय है, बजाय अनिवार्य? यदि सरकार के पास सच्ची संवेदनशीलता और संवैधानिक प्रतिबद्धता होती, तो दलित महिलाओं की सुरक्षा, एफआईआर स्वतः दर्ज करना, गवाहों की सुरक्षा — ये प्राथमिक नीतियाँ तुरंत और कठोरता से लागू होतीं। चुप्पी, विलम्ब और संवाद-विराम से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुवादी वर्गीय सत्ता संरचनाएँ राजनीतिक सत्ता को नियंत्रित कर रही हैं और उन्हें चुनौती देने वालों को लगातार दबाया जा रहा है।
रणनीति और न्यायोन्मुख सुझाव: व्यवस्थागत परिवर्तन की आवश्यकता
इस संरचनात्मक हिंसा को रोकने और दलितों को न्याय दिलाने के लिए, अब कठोर नियोजनात्मक सुझावों को तत्काल लागू करने की आवश्यकता है।
सबसे पहले, स्वचालित FIR और ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था हो ताकि दलितों की शिकायतें बिना किसी बाधा या पुलिसिया पक्षपात के तुरंत दर्ज हों, और PoA Act की व्यवस्था स्वतः लागू हो।
दूसरा, गवाह संरक्षण और स्वतंत्र नोडल एजेंसियाँ स्थापित की जाएँ, ताकि पीड़ित और गवाहों को पूर्ण सुरक्षा, आर्थिक सहायता और गुमनामी का विकल्प मिले, जिससे वे बिना किसी डर के गवाही दे सकें।
तीसरा, न्यायालयों में विशेष त्वरित फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित हों, जो दलित अत्याचार मामलों को अधिकतम तीन से छः महीने की निश्चित समय सीमा में निपटाएँ।
चौथा, पुलिस और प्रशासन में संवेदनशीलता प्रशिक्षण और जवाबदेही तंत्र स्थापित किया जाए, जिसमें जातिगत पूर्वाग्रह (बायस) हटाने के लिए नियमित और कठोर ट्रेनिंग हो और लापरवाही के लिए उच्चाधिकारियों की भी समीक्षा की जाए।
पाँचवाँ, पब्लिक ट्रांसपेरेंसी और निगरानी आवश्यक है, जहाँ राज्य-वार, वर्ष-वार मामलों की रिपोर्टें पारदर्शी हों और नागरिक समाज एवं मीडिया को उन्हें मॉनिटर करने की पूरी स्वतंत्रता मिले।
अंततः, दलित सशक्तिकरण कार्यक्रमों का आर्थिक आधार मजबूत किया जाए, जिसमें भूमि अधिकार, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ विशेष प्राथमिकता से लागू हों। यह स्पष्ट है कि यह सिर्फ “कुछ दोषी” की समस्या नहीं, बल्कि इतिहास-आधारित, संरचनात्मक मनुवादी शक्तियाँ हैं जो राजनीतिक चुप्पी और प्रशासनिक अनिच्छा के कारण मजबूत हो रही हैं।