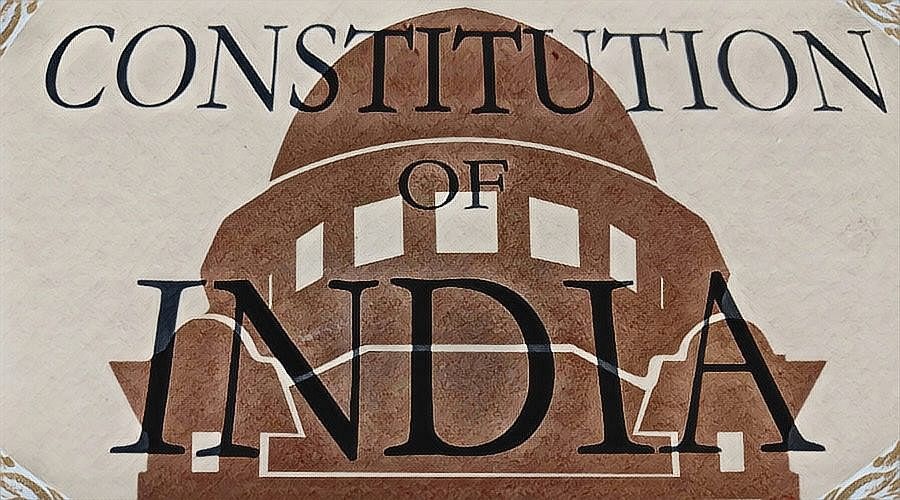नई दिल्ली 12 अक्टूबर 2025
भारत का संविधान, जो आज़ादी के बाद से देश को हर राजनीतिक और सामाजिक संकट में दिशा और स्थिरता प्रदान करता रहा है, आज स्वयं ही गहरे संकट के दौर से गुज़र रहा है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में न्यायपालिका, विशेषकर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की भूमिका पर एक तीखा और महत्त्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। जब लोकतंत्र के प्रहरी संस्थानों पर सुनियोजित ढंग से दबाव बनाया जा रहा हो, उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हों, तब यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या CJI को एक नैतिक प्रतिरोध दर्ज नहीं कराना चाहिए था? संविधान पर प्रत्यक्ष हमले के समय CJI का इस्तीफ़ा महज़ एक व्यक्तिगत या प्रशासनिक निर्णय नहीं होता; यह राष्ट्रीय नैतिक जागरण का एक शक्तिशाली प्रतीक बन सकता था, जो सत्ता को संविधान की गरिमा के सामने झुकने पर मजबूर कर देता, और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक मिसाल कायम करता। यह केवल कानून की नहीं, बल्कि नैतिक नेतृत्व की मांग थी, जिसे पूरा करने में हुई चूक को इतिहास शायद एक बड़ी ऐतिहासिक चूक के रूप में दर्ज करे।
संस्थागत मौन का युग और संवैधानिक आत्मा की सुरक्षा
पिछले कुछ वर्षों में, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, और मीडिया जैसे महत्त्वपूर्ण संस्थानों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर बार-बार गंभीर प्रश्न उठे हैं, जो लोकतांत्रिक संतुलन को बिगाड़ने का संकेत देते हैं। कानूनविदों और संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह वह दौर था जब न्यायपालिका को केवल कानूनी निर्णय देने की अपनी पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर, संविधान की आत्मा की सक्रिय रूप से रक्षा करने का दायित्व निभाना चाहिए था।
एक वरिष्ठ अधिवक्ता के शब्दों में, “अगर मुख्य न्यायाधीश ने उस निर्णायक क्षण में खड़े होकर यह घोषणा की होती कि वह संविधान की गरिमा की रक्षा के लिए पद छोड़ते हैं, तो यह कदम पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को झकझोर देता और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने का स्पष्ट संदेश देता।” यह कृत्य पूरे देश को एक स्पष्ट संदेश देता कि न्यायपालिका सत्ता के दबाव से पूरी तरह ऊपर है और देश में संविधान ही सर्वोच्च है, न कि कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल। संस्थागत मौन, इस संदर्भ में, केवल निष्क्रियता नहीं, संवैधानिक मूल्यों की उपेक्षा और अधिकारवाद के सामने आत्मसमर्पण का एक गहरा प्रतीक बन जाता है, जिसकी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ सकती है।
बिहार का चुनावी गणित: ‘वोट इंजीनियरिंग’ का गंभीर आरोप और न्यायपालिका की भूमिका
बिहार की हालिया राजनीतिक हलचलों ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी गंवेदनशील संदेह उत्पन्न किए हैं। विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए ‘वोट इंजीनियरिंग’ के दावों और अन्य आंकलनों के अनुसार, सत्ताधारी दल ने कथित तौर पर लगभग एक करोड़ वोटों के समीकरण को अपने पक्ष में मोड़ने का प्रयास किया—जिसमें करीब 67 लाख विपक्षी वोटों को काट कर 33 लाख अपने पाले में जोड़ने का प्रयास समझ में आता है। यह आंकलन समझें तो लगता है कि हर जिले में औसतन 20,000 वोट का एक पूर्वनिर्धारित लाभ तैयार किया गया है। इस विशेष रिपोर्ट में बिहार की स्थिति को शामिल करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह केवल चुनावी धांधली का मामला नहीं है, बल्कि यह प्रदर्शित करता है कि अदालत के बार-बार आदेशों और दिशानिर्देशों के बावजूद चुनाव प्रक्रिया में व्यापक गड़बड़ियाँ अब भी मौजूद हैं।
गड़बड़ियाँ इतनी विकराल और सुनियोजित हैं कि इन्हें केवल प्रशासनिक अक्षमता नहीं, बल्कि एक जानबूझकर किया गया कृत्य समझा जाना चाहिए, जिसका सीधा उद्देश्य लोकतंत्र की नींव को कमज़ोर करना है। अगर ये आरोप और शंका सत्य साबित होते हैं, तो यह घटना “लोकतंत्र में एल्गोरिद्म की सुनियोजित सेंध” को सिद्ध कर सकती है।
एक पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी इस संदेह को और मज़बूत करती है: “कुछ हज़ार वोटों का सुनियोजित अंतर भी सत्ता पलट सकता है। यह न केवल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रहार है, यह मतदाता के भरोसे को भी तोड़ती है।” यह स्थिति चुनावी लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को चुनौती देती है और सर्वोच्च न्यायालय के लिए यह एक नैतिक आह्वान था कि वह इन जानबूझकर की गई गड़बड़ियों पर निर्णायक स्टैंड लेता, ताकि चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बहाल हो सके।
‘जूता कांड’—एक प्रतीकात्मक हमला और साजिश का हिस्सा
हाल ही में हुई ‘जूता कांड’ की घटना को भी विश्लेषक एक सामान्य आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसे एक गहरी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना संविधान का अपमान करने वाली एक व्यापक राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य जनता के मन में संविधान की गरिमा पर प्रश्नचिह्न लगाना था। यह एक प्रतीकात्मक हमला था—संविधान को खुले तौर पर अपमानित करने का प्रयास, ताकि उसकी सर्वोच्चता और पवित्रता पर जनता का भरोसा टूट जाए।
इस पूरे घटनाक्रम में, सोशल मीडिया ट्रोल्स, ट्रोल नेटवर्क और राजनीतिक प्रचारतंत्र का समन्वय साफ़ दिखाई देता है, जो यह दर्शाता है कि यह एक सुनियोजित अभियान था। यह वही इकोसिस्टम है जो धीरे-धीरे जनता की संवैधानिक चेतना को धुंधला कर देना चाहता है और उन्हें संवैधानिक मूल्यों से विमुख कर रहा है, ताकि असंवैधानिक विचारधारा को आसानी से स्थापित किया जा सके। ऐसे प्रतीकात्मक हमलों का उद्देश्य वैचारिक वर्चस्व स्थापित करना और लोकतांत्रिक विमर्श को दूषित करना होता है।
CJI का संभावित नैतिक विद्रोह: एक कल्पना जो इतिहास बदल सकती थी
अगर उस निर्णायक क्षण में, मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय कक्ष में खड़े होकर यह ऐतिहासिक घोषणा की होती, “मैं संविधान की अवमानना के विरोध में तत्काल इस्तीफ़ा देता हूँ, और अब बिना सरकारी वाहन लिए पैदल अपने घर जाऊँगा,” तो यह दृश्य इतिहास में अमर हो जाता। ऐसा नैतिक साहस केवल सत्ता को ही नहीं झकझोरता, बल्कि समाज के हर वर्ग—दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, छात्रों, वकीलों—को संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित करता और एक राष्ट्रव्यापी संवैधानिक आंदोलन को जन्म देता। यह कदम संविधान बनाम मनुस्मृति, यानी बराबरी बनाम विशेषाधिकार की वैचारिक जंग का निर्णायक मोड़ बन सकता था, जहाँ न्यायपालिका ने स्वयं को केवल कानून की व्याख्या तक सीमित न रखकर नैतिकता के सर्वोच्च संरक्षक के रूप में स्थापित किया होता। यह नैतिक कार्रवाई देश को एक नई दिशा देती, जहाँ पद की गरिमा व्यक्तिगत सुविधा से ऊपर होती।
मौन भी एक अपराध है और नैतिक विद्रोह की आवश्यकता
वर्तमान राजनीति केवल वोटों की लड़ाई नहीं, बल्कि वैचारिक टकराव का मैदान बन चुकी है—यह संविधान बनाम मनुस्मृति, बराबरी बनाम विशेषाधिकार, और लोकतंत्र बनाम वर्चस्ववाद की लड़ाई है। संविधान का सम्मान केवल शब्दों या ग्रंथों में नहीं, बल्कि उन संस्थाओं की हिम्मत में निहित है जो उसे वास्तव में जीवित रखती हैं। जब संस्थाएँ चुप हो जाती हैं, तो संविधान केवल एक ग्रंथ बनकर रह जाता है, जिसके पास जनता को प्रेरित करने और अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की शक्ति नहीं बचती। यह सवाल अब भी प्रासंगिक है: क्या CJI का इस्तीफ़ा लोकतंत्र की रक्षा करता, या केवल एक प्रतीक बनकर रह जाता?
विशेषज्ञ मानते हैं कि भले ही इससे तत्काल सत्ता परिवर्तन न होता, लेकिन यह जनता में संवैधानिक नैतिकता का विस्फोट कर देता, जिससे हर नागरिक यह समझता कि संविधान केवल शासन की किताब नहीं, जनता की आत्मा है। मौन भी कभी-कभी नैतिक अपराध बन जाता है। भारत का संविधान समानता, न्याय और स्वतंत्रता का प्रतीक है, और उस पर हमला केवल क़ानूनी नहीं—यह एक गहरा नैतिक और सामाजिक संकट है। “जब न्याय मौन हो जाता है, तो इतिहास उसे क्षमा नहीं करता। और जब एक व्यक्ति बोलता है, तो पूरी पीढ़ियाँ जागती हैं।” न्यायपालिका आज भी देश की उम्मीद की अंतिम किरण है, लेकिन जब उस पर भी साया पड़ने लगे, तो नैतिक विद्रोह ही सर्वोच्च न्याय बन जाता है।
लेखक का दृष्टिकोण: लोकतंत्र की आत्मा के पक्ष में
यह रिपोर्ट किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ दुर्भावना से प्रेरित नहीं है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र की आत्मा के पक्ष में एक गंभीर और आवश्यक आह्वान है। यह संस्थागत साहस की मांग करती है, जो यह सुनिश्चित कर सके कि भारत का लोकतांत्रिक ढाँचा हर दबाव के सामने अटल रहे और नैतिकता की सर्वोच्चता कायम रहे। यह उस आदर्श की स्थापना के लिए है जहाँ देश का सर्वोच्च न्यायिक पद, संविधान की रक्षा के लिए, निजी हित और पद की सुविधा का त्याग करने को भी तैयार हो।