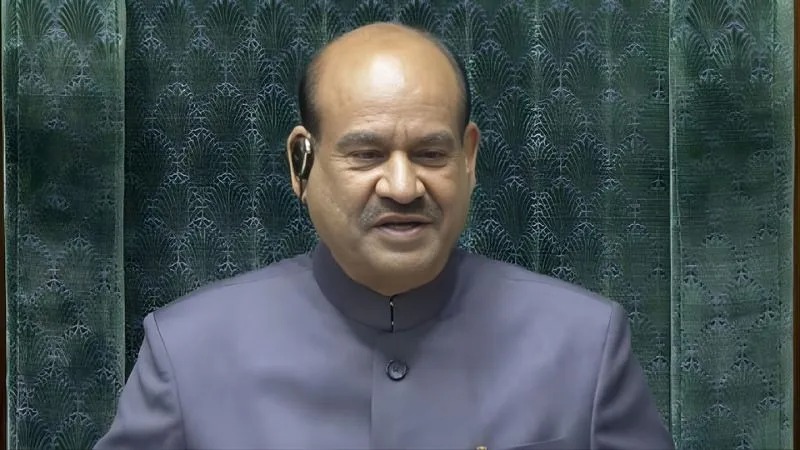नई दिल्ली/ पटना 9 अक्टूबर 2025
कागज़ पर अमीरी, ज़मीन पर फकीरी — बिहार के बजट का झूठ सुशासन
बिहार का 2025–26 का बजट ₹3.17 लाख करोड़ का आंकड़ा सुनने में भव्य और आशाजनक लगता है, पर इस भव्यता की परदे के पीछे छिपी कहानी घोर विडम्बना से भरी हुई है; सरकारी रिकॉर्ड और ऑडिट रिपोर्ट यही बताती हैं कि पैसे की कमी नहीं, उसके उपयोग की विफलता और प्रशासनिक जटिलताएँ हैं।
पिछले वर्षों में राजस्व और पूंजीगत व्ययों में जो करोड़ों-करोड़ रूपये अनुत्पादक रूप से लौटे या मात्र कागज़ों पर पड़े दिखे — वह केवल एक तकनीकी अक्षमता नहीं, शासन-प्रक्रिया और नीयत पर बड़ा सवाल है। जब राज्यों के विकास को तोलने के लिये बजट और उसके व्यय को प्राथमिक संकेत माना जाता है, और उसी बजट का बड़ा हिस्सा बिना उत्पादन के लौट जाता है, तो यह संकेत मिलता है कि निर्णय लेने वाले तंत्र — नीतियाँ, विभागीय कार्यान्वयन, और निगरानी — या तो सुस्त हैं या जानबूझकर नाकाम शोरगुल में बह रहे हैं।
ऐसे में ‘पैसा नहीं है’ का सरकारी विवरण केवल बहाना बनकर रह गया है; असली समस्या यह है कि पैसा जहाँ होना चाहिए वहाँ पहुँचकर ज़मीन पर परिणाम नहीं दे पा रहा — न स्कूलों में अध्यापक, न अस्पतालों में डॉक्टर, न गाँवों में नज़र आने वाला इंफ़्रास्ट्रक्चर। इस असंगति का मतलब साधारण-सा है: बड़े-बड़े संख्यात्मक बजट के बावजूद जनता को उस रकम का लाभ महीनों या वर्षों तक नहीं मिल पाता — और यही बिहार की सच्ची विडंबना बन चुकी है।
योजनाओं के क्रियान्वयन के नाम पर भ्रष्टाचार
MGNREGA, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी योजनाएँ जिनको सीधे जनता की रोज़मर्रा ज़रूरतों से जोड़ा गया था, आज वे ही सरकारी बिलों और स्थानीय ठेकेदारों की खपत का साधन बन चुकी हैं; जहाँ शुरू-शुरू में ये योजनाएँ सामाजिक सुरक्षात्मक कवच थीं, वहीँ अब उनमें फर्जी बिलिंग, अधूरे प्रोजेक्ट और धीमी भुगतान प्रक्रिया आम बात बन गई है। गरीब मजदूरों को काम करवा कर महीनों तक मजदूरी न मिलना, स्कूलों को वितरित फंडों का केवल कागज़ों पर दिखना, और अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी — ये सब संकेत करते हैं कि सिस्टम ने योजनाओं के उद्देश्य से ध्यान हटाकर वित्तीय मशीनरी के इर्द-गिर्द अपना खेल बना लिया है।
एक परियोजना पर आवंटित धन अगर सही समय पर और पारदर्शी तरीके से उपयोग नहीं होता, तो वह परियोजना शाश्वत रूप से विफल हो सकती है; बिहार में यही हो रहा है — करोड़ों रू. के आवंटन हैं, और स्थानीय लाभार्थियों की जेबों में लाभ नहीं। यह केवल प्रशासनिक सुस्ती नहीं, बल्कि कई बार सामंती संरचना, ठेकेदार-प्रणाली और राजनीतिक संरक्षण के कारण योजनाएँ जनता के लिए बेकार साबित हो जाती हैं। क्रियान्वयन का यह पतित चेहरा दिखाता है कि योजना बनाने वाले मन्त्रियों और नीति निर्माताओं के नारे और ज़मीन पर काम अलग-अलग डायरेक्शन में चलते हैं।
पटना और बाकी बिहार के बीच खाई गहरी
यदि आप बिहार के नक्शे पर आँख घुमा कर देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि विकास का केन्द्र पटना और उसके आसपास के कुछ जिलों तक ही सीमित रह गया है, जबकियों बाकी बड़े हिस्से—पूर्व, उत्तर तथा दक्षिणी जिलों में आज भी आधारभूत सुविधाओं, रोजगार के अवसरों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है; इस असमानता का अर्थ केवल आर्थिक विभाजन नहीं है, बल्कि सामाजिक गतिशीलता, अवसरों की उपलब्धता और जीवन की गुणवत्ता में भारी अंतर है।
पटना का प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा चमकता है, मगर उसी राज्य के कई हिस्सों में प्रति व्यक्ति आय इतनी कम है कि वहाँ के लोग आज भी बुनियादी उपभोग और स्वास्थ्य-शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। युवा वर्ग जो रोजगार के नाम पर पलायन कर रहा है, वही बिहार की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है — हर साल लाखों लोग बेहतर जीवन की तलाश में राज्य छोड़ रहे हैं, जिससे स्थानीय प्रतिभा और श्रमशक्ति का घोर क्षरण हो रहा है। यह विफलता बताती है कि नीतियाँ समावेशी नहीं रहीं — संसाधन सुस्पष्ट नीतियों के अभाव में केन्द्रों में जमा होते रहे और ग्रामीण/पश्चिमी जिलों तक उनकी पहुँच नहीं हो पाई। जब किसी राज्य का विकास सिर्फ़ राजधानी तक सीमित रहे तो वह राजनैतिक संतुलन और सामाजिक समरसता दोनों को चोट पहुँचाता है।
बुनियादी ढाँचे का त्रासदीपूर्ण पतन
जब पुल बनते हैं और वे बार-बार गिरते हैं, तो यह सिर्फ़ निर्माण-तकनीक की विफलता नहीं रह जाती — यह सिस्टम में मौजूद गड़बड़ी, ठेकेदार-नीती और गुणवत्ता नियंत्रण के अभाव का परोक्ष सबूत बन जाता है। अगुआनी-सुल्तानगंज जैसे महँगे प्रोजेक्ट का बार-बार ध्वस्त होना दर्शाता है कि सामग्री, निरीक्षण, अनुबंध प्रबंधन और, ज़ाहिर है, जवाबदेही के स्तम्भ कहाँ-कहाँ टूट रहे हैं। हर बार गिरने पर जांच बैठती है, आयोग बनते हैं, लेकिन संरचनात्मक सुधार और दोषी के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं होती; परिणाम यह होता है कि वही लोग फिर नए ठेके हासिल कर लेते हैं और चक्र फिर वहीँ घूमता है।
इस चक्र का सबसे बड़ा शिकार आम आदमी है — पुल के साथ-साथ पुल पर निर्भर व्यवसाय, यातायात और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी डगमगा जाती है। बुनियादी ढांचे की इस दुर्दशा के पीछे केवल भ्रष्टाचार ही नहीं, बल्कि निरीक्षण के ढाँचे में रुढ़ व्यवहार, अनुबंध-निविदा प्रक्रियाओं में छुपी अनियमितताएँ और स्थानीय प्रशासन की नाकामी भी है।
सत्ता बचाने के लिए जनता का भविष्य दांव पर
नीतीश कुमार का राजनीतिक सफ़र, जो अनेक गठबंधनों और उतार-चढ़ाव से भरा रहा, यह दर्शाता है कि सत्ता में टिके रहने की रणनीति अक्सर लंबे समय पर विकास को वेग देने के बजाय उसे धीमा कर देती है। मुफ्त योजनाओं और चुनावी वादों की प्राथमिकता ने तत्काल जनसमर्थन दिलाया होगा, पर यह समर्थन स्थायी आर्थिक आधार नहीं बना पाता जब तक अर्थव्यवस्था में नई उत्पादन इकाइयां, उद्योग और निवेश स्थापित न हों।
परिणामस्वरूप राज्य का कर्ज़ बढ़ता गया और 2025 तक जो ऋण-संतुलन बिगड़ा, उससे भविष्य की पीढ़ियों के उपर वित्तीय बोझ बढ़ गया। कर्ज का यही ढेर तब तक नियंत्रित नहीं होगा जब तक राजस्व-उत्पादन और पूंजीगत निवेश के स्थायी स्रोत नहीं बनते — और उसका अभाव सीधे तौर पर रोज़गार-निर्माण और स्थायी वृद्धि को प्रभावित करता है। राजनीति में वोट-बैंक प्रथाओं पर शासित नीतियाँ अक्सर तात्कालिकता पर केंद्रित रहती हैं, जबकि दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति और संस्थागत सुधार पीछे छूट जाते हैं — और बिहार इस ढाँचे की उपज बनकर उभरा है।
कुछ उपलब्धियाँ, पर व्यापक संदर्भ में अपर्याप्तता
न्यायपूर्वक यह मानना होगा कि नीतीश के शुरुआती कार्यकालों में कुछ ठोस सुधार दिखे — बिजली का विस्तार, सड़कों का निर्माण, कानून-व्यवस्था में बेहतर संकेत और साइकिल जैसी लड़कियों को सशक्त करने वाली योजनाएँ — ये सब प्रारम्भिक साख दे चुकी थीं। मगर सफलता का नया पैमाना तब बनता है जब वे सुधार समय के साथ अक्षय होकर व्यापक आर्थिक परिवर्तन में बदल जाएँ; बिहार में पिछले दशक में वही प्रारम्भिक लाभ स्थिर होते हुए रुकावट में बदल गए।
अन्य राज्यों के तुलनात्मक उन्नयन ने यह दिखा दिया है कि एक बार प्रारम्भिक सुधारों के बाद निरंतर निवेश, मानव संसाधन विकास और औद्योगिक नीतियों की मजबूती न होने पर राज्य पिछड़ सकता है। उपलब्धियाँ सच हैं, पर वे समग्र तस्वीर में टिकाऊ नहीं रहीं — और यही सबसे चिंतनीय बात है।
‘स्पेशल स्टेटस’ नहीं, सख्त जवाबदेही चाहिए
ABC एक्सक्लूसिव के तौर पर यह स्पष्ट कहना होगा कि बिहार की मौजूदा चुनौती वित्तीय सहायता की कमी से बड़ी है; इसे राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही की सख्ती चाहिए — पारदर्शी लेखा-परीक्षण, समयबद्ध उपयोगीकरण, ठेकेदारों और बाबुओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही, और जिला-स्तर पर लक्षित निवेश जो पलायन को रोक सके।
2025 का विधानसभा-चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का प्रश्न नहीं रहा; यह तय करेगा कि क्या बिहार अगली पीढ़ियों के लिये विकास का दीर्घकालिक आधार बना पाएगा या फिर 20 साल के कुशासन के साइलेंट कॉपी-पेस्ट पर ही और वर्षों तक टिका रहेगा। जनता का फैसला अब निर्णायक होगा — और उसी फैसले में निहित है कि क्या बिहार ‘रफ्तार’ पर लौटेगा या ‘रुकावट’ में ही फँसा रहेगा।