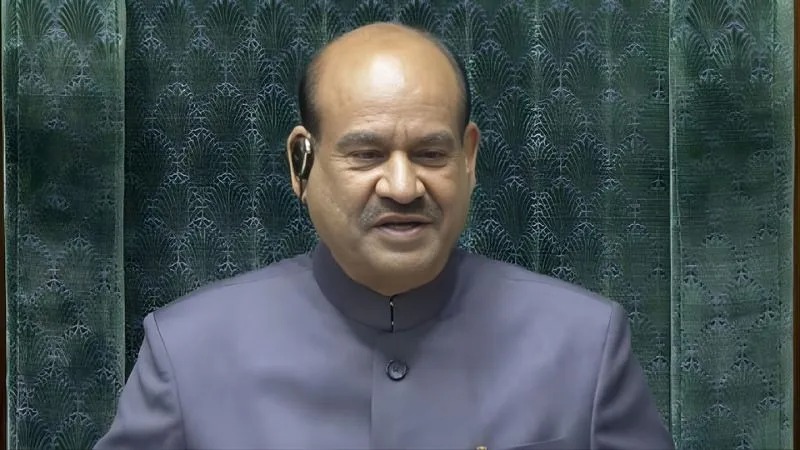वात्स्यायन का संदेश — आनंद पाप नहीं, आत्मा की भाषा
आज के भारतीय समाज में, जहाँ संस्कारों की आड़ में स्त्री के आनंद, उसकी इच्छा और उसके यौन अधिकारों पर बात करना आज भी एक सामाजिक निषेध (Taboo) माना जाता है, वहाँ यह याद रखना आवश्यक है कि इसी भूमि पर कभी प्रेम को पूजा का रूप और शरीर को आत्मा का मंदिर कहा गया था। यह एक बड़ी विडंबना है कि जो बातें आज हमें ‘शर्मनाक’ या ‘अश्लील’ लगती हैं, वे कभी भारतीय सभ्यता का सबसे सुंदर, सहज और स्वाभाविक हिस्सा थीं, जिन्हें जीवन की संपूर्णता के लिए आवश्यक माना जाता था। लगभग दो हज़ार साल पहले, तीसरी शताब्दी ईस्वी के आस-पास, जब दुनिया के अधिकांश हिस्से इन विषयों पर मौन थे, तब भारत में वात्स्यायन मल्लनाग नामक एक गहन विचारक ने संस्कृत में एक अद्भुत और कालजयी ग्रंथ लिखा — कामसूत्र। यह ग्रंथ दृढ़ता से घोषणा करता है कि काम केवल देह की भाषा नहीं है, यह आत्मा का अनुभव है, एक आध्यात्मिक साधना।
वात्स्यायन ने इसे मात्र यौन क्रिया का विज्ञान नहीं माना, बल्कि जीवन के चार मूलभूत पुरुषार्थों — धर्म (कर्तव्य), अर्थ (धन), काम (आनंद), और मोक्ष (मुक्ति) — को पूर्ण करने के लिए ‘काम’ को एक अनिवार्य और सम्मानित स्थान दिया। उनका स्पष्ट मत था कि “आनंद धर्म का साथी है; बिना आनंद के जीवन अधूरा है,” क्योंकि यह आनंद ही मनुष्य की प्राकृतिक ऊर्जा है जो उसे जीवन जीने की शक्ति और उत्साह प्रदान करती है।
कामसूत्र की रचना — देह से परे, मन और आत्मीयता का विज्ञान
कामसूत्र की गहराई और विशालता को अक्सर गलत समझा गया है। यह ग्रंथ कुल 7 भाग, 36 अध्याय और लगभग 1250 श्लोकों में फैला हुआ है, लेकिन इनमें से केवल 20% हिस्सा ही यौन मुद्राओं या तकनीकों पर केंद्रित है; जबकि शेष 80% हिस्सा प्रेम के दर्शन, सभ्य सामाजिक व्यवहार, शालीनता, गहरे संवाद और 64 कलाओं के महत्व पर आधारित है।
वात्स्यायन ने प्रेम को केवल एक जैविक या सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि की कला माना — ठीक संगीत, नृत्य, चित्रकला और काव्य की तरह। उनका मानना था कि प्रेम को पूरी गहराई और सुंदरता के साथ जीने के लिए व्यक्ति को 64 कलाओं (गांधारी कलाएँ) का ज्ञान होना चाहिए, जिनमें वाद्य यंत्र बजाना, परफ्यूम बनाना, फूलों को सजाना, कविता कहना, वार्तालाप की कला, वस्त्रों का सही संयोजन, और यहाँ तक कि खेल और जादू तक शामिल थे।
इन कलाओं का मूल उद्देश्य यह था कि वे प्रेमी-प्रेमिका के बीच प्रेम को एक निरंतर संवाद बनाए रखें, रिश्ते को भौतिक सीमाओं से ऊपर उठाकर भावनात्मक और बौद्धिक रूप से जीवंत बनाए रखें। इस गहन दृष्टिकोण से देखें तो कामसूत्र महज़ एक ‘सेक्स मैनुअल’ नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, आत्मीयता और प्रेम की आध्यात्मिक यात्रा का दर्शनशास्त्र है, जो मानता है कि देह का संबंध तभी अर्थपूर्ण हो सकता है, जब वह मन और आत्मा के संवाद और सहमति में ढल जाए।
आसनों का रहस्य — भावनाओं का नृत्य, संतुलन और समानता का प्रतीक
कामसूत्र में वर्णित 64 आसन या मुद्राएँ केवल शारीरिक गतिविधियाँ नहीं हैं, बल्कि ये प्रेमियों के बीच भावनाओं की अभिव्यक्ति, विश्वास और गहरे संतुलन की भाषा हैं। इन आसनों को मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक प्रतीकों के रूप में देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, संयोग आसन (आमने-सामने) केवल एक सरल मुद्रा नहीं है; यह समानता, आपसी सम्मान और पारदर्शिता का प्रतीक है, जहाँ दोनों प्रेमी एक-दूसरे की आँखों में झांकते हैं, जो यह संकेत देता है कि शारीरिक मिलन से पहले मन का मिलन और भावनात्मक जुड़ाव स्थापित हो चुका है।
इसी तरह, विपरीत आसन (जहाँ स्त्री अग्रणी हो) उस समय की सामाजिक रूढ़ियों पर एक मौन और शक्तिशाली विद्रोह था। यह स्त्री की स्वतंत्रता, उसकी इच्छा और उसके नियंत्रण का उत्सव है। वात्स्यायन ने इस आसन को प्रोत्साहित करते हुए स्पष्ट किया कि प्रेम का सौंदर्य तभी पूर्ण होता है, जब स्त्री भी अपने सुख और क्रिया में समान व अग्रणी भूमिका निभाए। इसके अलावा, आलिंगन और चुंबन की मुद्राएँ केवल स्पर्श नहीं हैं, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक तैयारी, भावनात्मक सामंजस्य और विश्वास का अभ्यास हैं।
10 प्रकार के आलिंगन और 8 प्रकार के चुंबन का विस्तृत वर्णन करके, कामसूत्र ने प्रेम को एक ऐसी ध्यानमय स्थिति तक पहुँचाने का प्रयास किया, जहाँ दोनों देह का अहंकार भूलकर एक-दूसरे के प्रति पूरी तरह सजग और करुणावान हो जाते हैं। इन सभी मुद्राओं का अंतिम संदेश यही है कि प्यार में कोई ऊँचा या नीचा नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं, और वात्स्यायन के शब्दों में: “प्रेम तभी पूर्ण होता है जब दोनों एक-दूसरे के आनंद में विलीन हो जाएँ; संतुलन ही प्रेम का धर्म है।”
स्त्री की स्वतंत्रता — कामसूत्र का मौन विद्रोह और सामाजिक उद्घोषणा
कामसूत्र की सबसे बड़ी क्रांतिकारी देन यह है कि इसने स्त्री की इच्छा और सुख को पुरुष की इच्छा के समकक्ष रखा। यह विचार उस युग में आया था जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में महिलाओं को संपत्ति या वस्तु से अधिक कुछ नहीं माना जाता था। वात्स्यायन ने निडर होकर लिखा: “स्त्री पहले तृप्त हो, क्योंकि वही सृजन की जननी है।” यह पंक्ति मात्र यौन दर्शन नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सामाजिक और सांस्कृतिक उद्घोषणा थी, जिसने स्त्री को जीवन के केंद्र में स्थापित किया — वह शक्ति जो आनंद देती भी है और नई सृष्टि का सृजन भी करती है।
ग्रंथ में स्त्रियों के लिए विशेष अध्याय समर्पित हैं, जिनमें उनकी शिक्षा, शृंगार, आकर्षण, भावनात्मक संवाद और स्वास्थ्य की चर्चा है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्राचीन भारत में ‘काम’ को पाप या शर्म का विषय नहीं, बल्कि जीवन की एक आवश्यक, पूजनीय और स्वस्थ ऊर्जा माना जाता था। यह उदार दृष्टि भारतीय सभ्यता के एक स्वर्णिम काल की झलक प्रस्तुत करती है, जहाँ प्रेम और आनंद को धर्म के ही एक रूप में स्वीकारा गया था।
सभ्यता का पतन — जब प्रेम को अपराध और अश्लीलता बना दिया गया
यह सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस सभ्यता ने प्रेम को साधना और पूजा कहा, उसी समाज ने बाद में इसे शर्म, पाप और अश्लीलता का विषय बना दिया। इस पतन की जड़ें मध्यकालीन धार्मिक रूढ़िवादिता और उसके बाद, विशेष रूप से, ब्रिटिश औपनिवेशिक नैतिकता (Victorian Morality) में गहरी हैं।
औपनिवेशिक शासकों ने कामसूत्र को ‘indecent’ (अश्लील) घोषित करके न केवल प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, बल्कि भारतीय समाज में ही इस ग्रंथ के प्रति एक गहरी हीनता और शर्म की भावना भर दी। जब 1883 में सर रिचर्ड बर्टन ने इसका विवादास्पद अंग्रेज़ी अनुवाद किया, तो पश्चिमी जगत में यह चर्चा का विषय तो बना, लेकिन वहाँ भी इसे इसकी आध्यात्मिकता को भुलाकर, मात्र एक ‘सेक्स गाइड’ के रूप में ही देखा गया।
इस प्रकार, पश्चिम ने उसमें केवल देह देखी और दर्शन को नज़रअंदाज़ कर दिया, और भारत ने शर्म के नाम पर अपने ही महान ज्ञान और सबसे उदार परंपरा को त्याग दिया। यह इतिहास का वह दुखद दौर था जब वह ग्रंथ जो आत्मा और देह के संतुलन की बात करता था, उसे समाज में अश्लीलता का प्रतीक बनाकर दबा दिया गया।
आधुनिक भारत में कामसूत्र — प्रेम और आत्मबोध का पुनर्जागरण
आज के अत्यधिक डिजिटल, तनावग्रस्त और सतही संबंधों के युग में, कामसूत्र पहले से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। यह ग्रंथ आज की पीढ़ी को याद दिलाता है कि आनंद कोई अपराध नहीं, बल्कि आत्म-सम्मान और आत्म-स्वीकृति की अभिव्यक्ति है। जब कोई व्यक्ति अपने शारीरिक और भावनात्मक सुख को स्वीकार करता है, तो वह केवल देह से नहीं, बल्कि समाज द्वारा थोपे गए झूठे नैतिक बंधनों से भी मुक्त होता है।
भारत ने कभी भी आनंद को दबाया नहीं — खजुराहो, कोणार्क और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियाँ कामसूत्र की जीवित, सांस लेती हुई प्रतियां हैं। ये मूर्तियाँ प्रेम, आध्यात्मिकता, और सृष्टि के उत्सव को एक साथ मनाती हैं। वात्स्यायन ने जो बात सदियों पहले लिखी थी, वह आज भी एक दर्पण है: “जब शरीर मौन हो जाए, आत्मा भी बोलना भूल जाती है।” यह पंक्ति आज हमें सिखाती है कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए, प्रेम और आनंद के संवाद को बनाए रखना अनिवार्य है।
प्रेम, धर्म और देह का त्रिवेणी संगम
कामसूत्र की असली सुंदरता यही है कि उसने मनुष्य को उसकी सबसे सच्ची पहचान दी — कि प्रेम केवल शब्द नहीं, बल्कि एक साधना है। जब प्रेम साधना बन जाता है, तब देह केवल स्पर्श का माध्यम नहीं रहती, बल्कि ध्यान का एक पवित्र स्थान बन जाती है। वात्स्यायन ने जिस ‘काम’ की बात की, वह क्षणिक वासना नहीं, बल्कि जीवन की चेतना और गहरी आत्मीयता थी।
इसलिए कामसूत्र आज भी हमारे समाज को यह संदेश देता है कि जो प्रेम को शर्म और वर्जनाओं से ढकता है, वह खुद जीवन के संपूर्ण आनंद और मुक्ति से दूर हो जाता है। और जो प्रेम को साधना बना लेता है, वही शरीर में आत्मा और आत्मा में शरीर का अनुभव कर पाता है। कामसूत्र का पुनर्जागरण केवल एक ऐतिहासिक चर्चा नहीं है, बल्कि यह आधुनिक समाज के लिए मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और भावनात्मक संवेदनशीलता का आधार बन सकता है।
आधुनिक भारत में कामसूत्र का पुनर्जागरण : जब आधुनिकता ने प्रेम को तोड़ा, तब कामसूत्र ने फिर जोड़ा
बीते कुछ दशकों में भारतीय समाज में आए अभूतपूर्व तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों ने रिश्तों को एक नई चुनौती दी है — तकनीक ने भावनाओं को ‘इमोज़ी’ में बदल दिया, और प्रेम को ‘स्वाइप’ की एक क्षणिक क्रिया में सीमित कर दिया। शहरों में रिश्ते बहुत तेज़ी से बनते और तेज़ी से टूटते हैं, जिससे युवाओं में मानसिक तनाव और भावनात्मक अस्थिरता बढ़ी है।
लेकिन इसी शोर और शॉर्टकट के युग में, कामसूत्र एक शांत, दार्शनिक फुसफुसाहट की तरह लौट आया है, जो कहता है: “प्यार को समझो, छुओ नहीं; प्रेम को जियो, दिखाओ नहीं।” आज के मनोवैज्ञानिक और संबंध विशेषज्ञ (Relationship Experts) यह मानते हैं कि वात्स्यायन का कामसूत्र केवल शारीरिक संबंधों का नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की एक उन्नत पाठशाला है।
यह सिखाता है कि किसी भी प्रेम संबंध में धैर्य, गहरा संवाद, और सम्मान सबसे बड़ी ‘कामनाएँ’ हैं — और बिना सच्ची भावनात्मक सहमति के किया गया कोई भी स्पर्श, प्रेम नहीं, बल्कि हिंसा या अपराध है।
सहमति (Consent): वात्स्यायन का दो हज़ार साल पुराना सिद्धांत
आज पूरी दुनिया में ‘सहमति’ (Consent) के सिद्धांत को यौन संबंधों की आधारशिला माना जाता है, जो आज के #MeToo और लैंगिक समानता (Gender Equality) के युग में सबसे शक्तिशाली सामाजिक अवधारणा बन गई है। लेकिन यह क्रांतिकारी विचार वात्स्यायन ने आज से दो हज़ार साल पहले ही अपने ग्रंथ में स्पष्ट रूप से रख दिया था।
उन्होंने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा: “जिससे बिना उसके मन के संपर्क किया जाए, वह काम नहीं, अपराध है।” वात्स्यायन का यह वाक्य दर्शाता है कि भारतीय दर्शन कभी भी पितृसत्तात्मक नहीं था, बल्कि उसने प्रेम को समानता और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में देखा। कामसूत्र की दृष्टि में, स्त्री केवल भोग की वस्तु नहीं है, बल्कि वह प्रेम की एक समान, स्वतंत्र और सम्मानित सहभागी है, जिसकी इच्छा और स्वीकृति सर्वोपरि है।
कामसूत्र और विज्ञान — मनोविज्ञान से भी आगे की दृष्टि
आज जब यौन शिक्षा को स्कूलों में धीरे-धीरे स्वीकृति मिल रही है, तब यह समझना महत्वपूर्ण है कि कामसूत्र ने केवल ‘Sex Education’ नहीं, बल्कि ‘Soul Education’ दी थी। इसने यौन संबंधों को केवल एक जैविक क्रिया नहीं, बल्कि एक जटिल मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया माना। वात्स्यायन ने बताया था कि प्रेम की शुरुआत ‘दृष्टि’ से होती है (नज़र से), फिर ‘वार्तालाप’ आता है, फिर ‘स्पर्श’, और उसके बाद ‘संयोग’।
ये चारों चरण सिखाते हैं कि प्रेम एक धीमी और सजग प्रक्रिया है — और वह सबसे सुंदर तब होता है जब उसमें धैर्य, गहरी समझ और करुणा शामिल होती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी इस बात की पुष्टि करती है कि प्रेम में आनंद देने वाले हार्मोन (जैसे ‘डोपामाइन’ और ‘ऑक्सीटोसिन’) तभी स्रावित होते हैं जब संबंधों में गहरी सुरक्षा और आपसी भरोसा होता है — ठीक वही बात जो वात्स्यायन सदियों पहले बता चुके थे।
स्त्री-पुरुष नहीं, ऊर्जा और संतुलन की बात करता है कामसूत्र
वात्स्यायन के लिए प्रेम का अर्थ केवल स्त्री और पुरुष का संबंध नहीं था; उन्होंने प्रेम को ऊर्जा के मिलन के रूप में देखा — जहाँ पुरुष की ‘शिव’ ऊर्जा (चेतना) और स्त्री की ‘शक्ति’ ऊर्जा (सृजन) का संतुलन होता है। इसलिए कामसूत्र में हर आसन केवल देह की मुद्रा नहीं, बल्कि एक दूसरे के बीच ऊर्जा के प्रवाह और आदान-प्रदान का माध्यम है।
आधुनिक योगशास्त्र और तंत्र दर्शन में भी यही विचार आगे बढ़ा कि प्रेम और ध्यान, दोनों की जड़ एक ही है — वह है एकाग्रता, सजगता और गहरा स्नेह। आज जब रिश्ते अस्थिर हैं, विवाह टूट रहे हैं और भावनाएँ उथली होती जा रही हैं, तब कामसूत्र हमें सिखाता है कि प्रेम को क्षणिक नहीं, बल्कि टिकाऊ और स्थायी बनाने के लिए केवल रोमांस नहीं, बल्कि रूहानी एकता और ऊर्जा का संतुलन ज़रूरी है।
कामसूत्र का आधुनिक अर्थ — प्रेम में स्वीकृति और आत्मबोध
आज के समाज में, जहाँ प्यार अक्सर एक प्रदर्शन बन गया है — सोशल मीडिया पर ‘परफेक्ट कपल्स’ की तस्वीरों में — कामसूत्र हमें सिखाता है कि प्रेम बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की सबसे गहरी अनुभूति है। यह कहता है कि सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने शरीर को समझते हैं, अपने साथी की भावनाओं को सुनते हैं, और अपने मन की इच्छाओं को स्वीकार करते हैं।
कामसूत्र आधुनिक समाज को यही सिखाता है — कि आनंद का अर्थ वासना नहीं, बल्कि आत्मबोध है। वह क्षण जब शरीर और आत्मा दोनों एक-दूसरे के प्रति पूरी तरह से सजग और स्वीकृत हो जाते हैं — वही सच्चा और संपूर्ण सुख है। कामसूत्र का पुनर्जागरण यही है — कि आज की पीढ़ी फिर से समझ रही है कि प्रेम केवल स्पर्श नहीं, एक साधना है। और जब प्रेम साधना बन जाए, तो शरीर ध्यान बन जाता है, और आत्मा — उसका उत्सव।